भारत और आसपास के बाढ़-प्रभावित इलाके
- Asliyat team
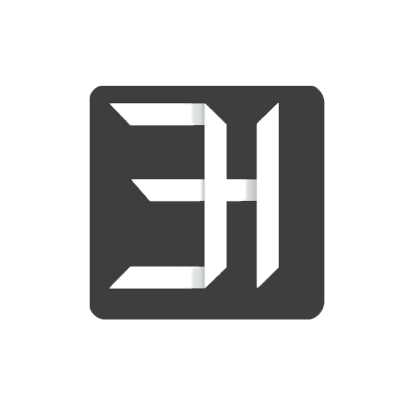
- Sep 5, 2025
- 4 min read
उत्तर भारत इस मानसून में पाँच दशकों के दूसरे सबसे अधिक वर्षामय सीज़न से गुजर रहा है। मौसम प्रणालियों की लगातार श्रृंखला ने हिमालयी और मैदान दोनों हिस्सों में असामान्य बारिश कराई है, जिससे व्यापक बाढ़, भूस्खलन और आधारभूत ढाँचे को भारी नुकसान हुआ है। हालिया आकलन के मुताबिक उत्तर भारत में वर्षा अधिशेष लगभग 37% तक पहुँच गया है, जो 1988 के बाद सबसे अधिक है।
उत्तर भारत: हिमाचल–पंजाब–हरियाणा–जम्मू–कश्मीर का संकट
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में लगातार बारिश और पहाड़ी ढालों पर ढहाव के कारण सैकड़ों जानें गईं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। तस्वीर साफ़ है: सड़कों के धंसने, पुलों के बहने और गाँवों के डूबने से जीवन-रेखा सेवाएँ बाधित हुई हैं। मीडिया संकलनों और आधिकारिक बयानों के आधार पर इन राज्यों में कुल मौतों का आँकड़ा कई सौ के पार जा चुका है, जबकि केवल पंजाब में ही सरकार ने कम-से-कम 30 मौतें और तीन लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि की है। राज्य के कृषि इलाकों में फ़सलों और पशुधन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने व्यापक तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने राज्य को वातावरणीय आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया, क्योंकि बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड में अब तक लगभग ₹3,526 करोड़ की क्षति हुई है तथा 341 लोगों की मौत हुई है। राज्यभर में 600 से अधिक सड़कों बंद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुल्लू–मनाली हाइवे का एक हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ है। हरियाणा में गग्गर नदी टूटने से फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जिलों में व्यापक बाढ़ आई है। लगभग 1.8 लाख एकड़ क्षेत्र पानी में डूब गया है और करीब 180 गाँवों में जलभराव हुआ। जम्मू एवं कश्मीर में हाल में भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसी दौरान বৈष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ जिसमें 6 लोगों की जान गई और यात्रा स्थगित कर दी गई। इसके अलावा, Supreme Court ने जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन और अवैध वनों की कटाई पर केंद्र और संबंधित राज्यों से जवाब मांगा है।

बाँध प्रबंधन और तात्कालिक खतरा
भाखड़ा बाँध का जलस्तर 1,678.97 फ़ुट तक पहुँचने पर प्राधिकरण ने दबाव घटाने के लिए 80–85 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया। नतीजतन रोपड़, नंगल और आनंदपुर साहिब के निचले इलाकों में बाढ़ का ख़तरा बढ़ा और प्रशासन ने निकासी सलाह जारी की। आपदा राहत बलों की टीमें तैनात हैं और कई स्कूल–समुदाय भवनों को अस्थायी शिविरों में बदला गया है।
दक्षिण भारत: तेलंगाना में ‘अभूतपूर्व’ बारिश के बाद बाढ़
25–28 अगस्त के बीच हुई तीव्र वर्षा से तेलंगाना के कई ज़िले जलमग्न हुए। राज्य सरकार ने केंद्र से ₹16,731 करोड़ की सहायता माँगी है, जिसमें तात्कालिक रूप से सड़क, रेल पटरी, कल्वर्ट और विद्युत ढांचे की मरम्मत प्राथमिकता है। प्रारम्भिक आँकड़ों के मुताबिक कम-से-कम 22 मौतें दर्ज हुईं और फसल–मकान–पशुधन हानि का आकलन जारी है।
पूर्वोत्तर: असम में चक्रवात ‘रेमल’ के बाद की बाढ़ और दीर्घकालिक जोखिम
सीज़न की शुरुआत में पूर्वोत्तर विशेषकर असम में चक्रवात ‘रेमल’ के बाद बाढ़ का दौर चला। सरकारी बुलेटिनों के अनुसार जून की लहर में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और मौतों का आँकड़ा दो दर्जन से ऊपर पहुँचा। कई जिलों में शहरी बाढ़ और भूस्खलन साथ-साथ देखे गए। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी की भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण बार-बार बाढ़ की चपेट में आता है—जिसका असर अबके साल भी स्पष्ट रहा।
सीमापार परिघटना: बांग्लादेश–पाकिस्तान में भी असर
भारत में भारी वर्षा और पहाड़ी नदियों के उफान का प्रभाव पड़ोसी देशों में भी दिख रहा है। उत्तरी बांग्लादेश में अगस्त के मध्य में तीस्ता और दूधकुमा जैसी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर जाने से एक लाख से अधिक लोग फँस गए और राहत–पुनर्वास की व्यापक आवश्यकता पैदा हुई। नदी-प्रणालियों का रुझान अगले कुछ दिनों में फिर बढ़ने का अनुमान भी जताया गया।
पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप भी सामने आए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मत है कि इस तरह के दावे भौगोलिक–हाइड्रोलॉजिकल वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते और जलवायु-परिवर्तन जनित चरम वर्षा की प्रवृत्ति पर ध्यान देना अधिक समीचीन है।
राहत, चुनौतियाँ और अगले 72 घंटे
एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की तैनाती, सामुदायिक आश्रयों और निकासी अभियानों के बावजूद चुनौती बड़ी है—क्योंकि पहाड़ी कटाव और लगातार भीगती मिट्टी से नए भूस्खलन का जोखिम बना रहता है। पंजाब–हिमाचल बेल्ट में शिक्षा संस्थान बंद करने, सरकारी आवासों को आश्रय केंद्र बनाने और त्वरित संचार व्यवस्थाएँ कायम रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के ‘रेड अलर्ट’ और बांधों से नियंत्रित जल-रिलीज़ संकेत देते हैं कि तराई–निचले क्षेत्रों में अगले 48–72 घंटे निगरानी और निकासी योजनाओं के लिए निर्णायक होंगे।
बड़ा परिप्रेक्ष्य: क्यों बढ़ रही है बाढ़ की तीव्रता
इस वर्ष उत्तर भारत में वर्षा अधिशेष, पश्चिमी विक्षोभ–मॉनसून इंटरैक्शन और ऊँचे कैचमेंट में उच्च-तीव्रता बारिश की आवृत्ति ने जोखिम को गुणा किया। जब ऊपरी बेसिन तेज़ी से पानी छोड़ता है और मैदानों में नदियाँ पहले से भरी हों, तो बाँध–बैरेजों पर ‘फ़्लड मैनेजमेंट’ की विंडो छोटी पड़ जाती है—जैसा कि भाखड़ा प्रणाली में देखने को मिला। कृषि कोण से देखें तो खरीफ़–धान, कपास, गन्ने और पशुधन पर क्षति दीर्घकालिक आय-हानि में बदलेगी, जिसके लिए विशेष इनपुट सब्सिडी, फसल-बीमा क्लेम के त्वरित निपटान और ग्रामीण सड़कों–बाज़ारों की शीघ्र बहाली जरूरी होगी।
क्या करें (सुझाव)
राज्यों को तात्कालिक राहत के साथ ‘रिस्क-इन्फॉर्म्ड’ पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी—बाढ़-सहिष्णु सड़कें, ऊँचे प्लेटफॉर्म पर सामुदायिक भवन, और खतरे की रियल-टाइम सूचना के लिए ग्राम-स्तरीय सिस्टम। पूर्वोत्तर और पंजाब–हरियाणा–यमुना–घग्घर बेल्ट में बाढ़-सहायक नक्शों का अद्यतन और नदीमैदानों में अनियोजित निर्माण पर सख्ती अब देर नहीं की जा सकती। साथ ही, सीमापार नदी-प्रबंधन (ब्रह्मपुत्र/तीस्ता) पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा-साझेदारी और पूर्व-सूचना तंत्र क्षेत्रीय जोखिम को घटा सकते हैं।







Comments